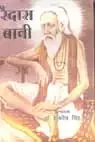|
जीवनी/आत्मकथा >> भये कबीर कबीर भये कबीर कबीरशुकदेव सिंह
|
93 पाठक हैं |
||||||
इस किताब में गवेषणा, पाठ-अनुसन्धान, प्रासंगिकता पर बहस है। विभिन्न कला माध्यमों में कबीर का दर्शन, प्रदर्शन और सामाजिक सुविधाओं के बाहर घूमते लोगों की निर्गुनियाँ व्यथा है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
कबीर को लेकर एक वैचारिक संसार का निर्माण हुआ है जिसे विश्वविद्यालयों के
अध्ययन में छोटे मुँह और बड़ी बात के रूप में स्थापित किया गया। एक दूसरी
दुनिया गायकों की है जो सड़क से लेकर ओमकारनाथ ठाकुर और कुमार गन्धर्व के
‘हममा, तुममा, सब मा, बहुरि अकेला’ के अकेलेपन में है
अथवा
‘जतन बताए जैहो, कइसे दिन कटिहैं।’ गंगा हो, चाहे
जमुना इनके
बीच में एक झोपड़ी बनाने के धुर पंचम सुर में भी कबीर को सुनना है। एक हद
तक वहाँ है जहाँ कबीर केवल सुनने की बात करते हैं, कहना हो ही नहीं सकता।
समझने की एक अन्तर्मुखी तड़प अर्थात् निरन्तर बैखरी से लौटते हुए परा तक
पहुँचने की भूमिका। इसे गूँगे का गुड़ या ‘समुझि मनहि
रहिए’
की दशा भी कहा जा सकता है।
इस किताब में गवेषणा, पाठ-अनुसन्धान, प्रासंगिकता पर बहस है। विभिन्न कला माध्यमों में कबीर का दर्शन, प्रदर्शन और सामाजिक सुविधाओं के बाहर घूमते लोगों की निर्गुनियाँ व्यथा है। मृत्यु के बहुत निकट जाकर ‘उलटभाषी’ को भी समझने की कोशिश की है।
कई तरह के पाठकों और विचारकों के लिए इस किताब में अलग-अलग पाठ हैं। सारे पाठ बाहर से अलग, भीतर से एक हैं। आधी शताब्दी की यह यात्रा इस विश्वास के साथ की गयी है कि ‘हम न मरिहै, मरिहैं संसारा’। संसार भी अपना हिन्दी वाला नहीं; सारी दुनिया—जिसे सरग-पताला कहा जाता है।
यह भी नहीं हो पाया कि कबीर बानी के कई रूप-रूपान्तर उनकी भाषा के राजस्थानी, पंजाबी, ब्रजी, अवधी, मैथिली, बुंदेली, मालवी, रूपों में अतः सूत्र क्या है ? ‘धुर पूरब’ का मतलब क्या है ? यह तय है कि कबीर ‘अर्थ’ के कवि है। किसी भी भाषा से उनका अर्थ नहीं मरता। वे एक तरह के वाद्य हैं, सबद है। वाद्य शब्दों की भाषा नहीं होती। वे लिंग, वचन, कारक और क्रिया में व्याकृत नहीं होते शुद्ध ‘सबद’ होते हैं। अर्थ भी, शब्द भी ; ‘अर्थात्’ नहीं। ये वाद्य-शब्द संगीत में खुलते हैं। विभिन्न रागों में इन सबद उक्तियों का गायन होता है। गूँगे के गुड़ और गूँगे की मिर्ची की तरह मीठा और तीता व्यक्त हो जाये, चेहरा ही बोल दे, लेकिन जीभ न बोल सके, ऐसी मृतजिह्व बानी के कवि कबीर सुर और तान की भंगिमाओं में सधते हैं। ‘सुनो भाई, के बाद साधो का अर्थ है, साधना करो, सिद्ध करो। सम्बोधन का अनुज्ञा लोट् में अर्थ तो रायपुर के भारती-बन्धु ही जानते हैं।
इस किताब में गवेषणा, पाठ-अनुसन्धान, प्रासंगिकता पर बहस है। विभिन्न कला माध्यमों में कबीर का दर्शन, प्रदर्शन और सामाजिक सुविधाओं के बाहर घूमते लोगों की निर्गुनियाँ व्यथा है। मृत्यु के बहुत निकट जाकर ‘उलटभाषी’ को भी समझने की कोशिश की है।
कई तरह के पाठकों और विचारकों के लिए इस किताब में अलग-अलग पाठ हैं। सारे पाठ बाहर से अलग, भीतर से एक हैं। आधी शताब्दी की यह यात्रा इस विश्वास के साथ की गयी है कि ‘हम न मरिहै, मरिहैं संसारा’। संसार भी अपना हिन्दी वाला नहीं; सारी दुनिया—जिसे सरग-पताला कहा जाता है।
यह भी नहीं हो पाया कि कबीर बानी के कई रूप-रूपान्तर उनकी भाषा के राजस्थानी, पंजाबी, ब्रजी, अवधी, मैथिली, बुंदेली, मालवी, रूपों में अतः सूत्र क्या है ? ‘धुर पूरब’ का मतलब क्या है ? यह तय है कि कबीर ‘अर्थ’ के कवि है। किसी भी भाषा से उनका अर्थ नहीं मरता। वे एक तरह के वाद्य हैं, सबद है। वाद्य शब्दों की भाषा नहीं होती। वे लिंग, वचन, कारक और क्रिया में व्याकृत नहीं होते शुद्ध ‘सबद’ होते हैं। अर्थ भी, शब्द भी ; ‘अर्थात्’ नहीं। ये वाद्य-शब्द संगीत में खुलते हैं। विभिन्न रागों में इन सबद उक्तियों का गायन होता है। गूँगे के गुड़ और गूँगे की मिर्ची की तरह मीठा और तीता व्यक्त हो जाये, चेहरा ही बोल दे, लेकिन जीभ न बोल सके, ऐसी मृतजिह्व बानी के कवि कबीर सुर और तान की भंगिमाओं में सधते हैं। ‘सुनो भाई, के बाद साधो का अर्थ है, साधना करो, सिद्ध करो। सम्बोधन का अनुज्ञा लोट् में अर्थ तो रायपुर के भारती-बन्धु ही जानते हैं।
मरिहैं संसार
जीवन की ओर से नहीं, मृत्यु की ओर से संसार को देखने वाले कबीर कई तरह से
पढ़े गये। मठों में बाबा की तरह जाने कब से, पंथों में पंथ गायक की तरह,
ग्रन्थों के विरोधी के रूप में, ना मुसलमान’ की तरह/आचार में
‘ना हिन्दू’ की तरह, गृहस्थों में साधु और साधुओं के
बीच
‘पकरि जुलाहा कीन्हा’ के व्यथावाचक की तरह सूफियों
में सूफी,
शहीद, मलामती पीर, मुर्शिद की भाँति। अगर कंठ में सुर हो, तान हो, लय हो
तो, सोलह रागों के राग, रागनियों, रंग और ठाट के सारे तुरुप में
एक
अनोखे निरगुनियाँ की पहचान लिए खुद कामगर, दस्तावेज लेकर भिखारियों और
साधुओं में कभी मांगते हुए और कभी देते हुए विरक्त की तरह। इसलिए
पचास-इक्यावन साल पहले मुझे बताया गया कि कबीर तमाम तरह की किताबों में
मिलेंगे लेकिन धूल में, मिट्टी में, दुःख में, विषाद में ही असल कबीर
मिलेंगे।
कहीं पाठ की समस्या है, कहीं अर्थ की। कहीं अर्थ के अर्थ की। इसी तरह कहीं वेदान्ती हैं, कहीं निहंग। छह सौ साल से कुछ ज्यादा वर्ष हुए कबीर सारी दुनियाँ में भाषा के आर-पार सारंगी के तार में, खँज़ड़ी की छेड़छाड़ में, पाँव के घुँघरू में, करताल, खड़ताल, रेबाब, किंगरी और कुकुही में वचन नहीं, वाद्य हैं।
ऐसे विलक्षण व्यक्ति को जो छह सौ वर्षों से निरन्तर बन रहा है और तब तक बनता रहेगा जब तक आदमी अपने को ढंकते हुए, उभारते हुए, डरते हुए, डराते हुए, निर्भय नहीं हो जायेगा। इस कबीर की तलाश में पचास सालों के लिखित कुछ नमूने इस किताब में बिना किसी क्रम के प्रस्तुत हो रहे हैं। इसे विषयबद्ध भी किया जा सकता था, क्रमबद्ध भी लेकिन कबीर का कोई क्रम बन ही नहीं सकता वे सिलसिले से समझे जाने योग्य रचनाकार नहीं हैं। इसालिए उनकी सही सार्थक पढ़ाई के लिए उनको पढ़ते हुए हर पन्ने का एहसास अलग होना चाहिए।
कहीं कविता की दुनिया के अन्तिम व्यक्ति, कहीं लोगों का मन ही नहीं; दाँत भी खट्टाकर देने वाला साहस। लेकिन कबीर के बिना काम नहीं चल सकता। उनकी रचना के भी कई हजार रूप हैं और विवेचना के भी कई-कई लेकिन दोनों स्तरों पर कबीर को रचना ही पड़ता है। क्योंकि हर व्यक्ति की रचनाशीलता में ही कबीर ही रचनाशीलता है। इस किताब के बहाने कबीर का पढ़ना पढ़ा जा सकता है।
क्या है कबीर का पढ़ना ? इसको देखना है तो दलित-संज्ञान के प्रतिष्ठित लेखक, विद्वान् आई.ए.एस. बार-बार अपने को दलित कहने वाले डॉ० धर्मवीर पढ़ना ही देख लिया जा सकता है। उन्होंने तीन किताबें ‘कबीर के आलोचक’ पुस्तक-माला के रूप में लिखी हैं। कबीर को पढ़ने वाला कोई नहीं छूटा लेकिन सभी उन्हें कबीर के आलोचक लगते हैं, अध्येता नहीं। उनकी सारी मेहनत इस बात के लिए है कि कबीर को किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा। किसी को उनसे यह भी पूछना चाहिए कि आपने कबीर को कितना पढ़ा ? कैसे पढ़ा ? साखी क्या है ? वह दोहा है या दोहा नहीं है? सबद क्या है? वह शब्द है या पद? या दोनों नहीं है? रमैनी क्या है? उसमें जो बातें लिखी गईं हैं उनमें किस तरह की कम्यता है। चांचर, बेइल, बिरहुली, विप्रमतीसी चौंतीसा कहरा, चैती घांटो, फाग, बसंत, जंजीरा क्या है? इंगला, पिंगला, सुखमन तार क्या है? जुलाहा, कसाई, साधु पांडे, काजी, मुल्ला भाई क्यों उनकी कविता में हैं? फिर राग सोरठा में क्यों वह कहते हैं
कि मैं तो बिगड़ गया तुम नहीं बिगड़ना, हरा भरा पेड़ था चन्दन के संग चंदन होकर बिगड़ गया। निर्मल जल था गंगा के संग गंगा होकर बिगड़ गया। लोहा था पारस के संग सोना होकर बिगड़ा। कबीर था ओछा कसब वाला जुलाहा, राम के संग राम होकर बिगड़ा। क्या है इसका मतलब ? यह तो नहीं कि कोई बनता नहीं, सभी बिगड़ते ही हैं। यह तो नहीं कि किसी तरह का कवि–समय या मिथक या विश्वास केवल सपना होते हैं सच नहीं। इस तरह कबीर कई बार पलट कर देखते हैं
और अंत में ‘आइला गवनवाँ की बारी’ के विदा का गीत गाते हैं विवाह के रूपक में मौत का मुखौटा लगाते हैं। ठीक से बैठने को ‘उनमनी’ और ‘उदासी’ कहते हैं। उनकी कविता दुनियाँ की ओर जाती है या स्वर्ग, हेवन या किसी स्तर पर दोजख की ओर जाती है। कबीर की कविता से जुड़े हुए बहुत छोटे-छोटे सवाल हैं ? इनको हल करने के लिए भी कबीर को कितने लोगों ने पढ़ा ? मैं तो चार दशक से ज्यादा कबीर को पढ़ाते हुए इन सवालों से ही जूझता रहा। डॉ० धर्मवीर से मैं यह जानना चाहूंगा कि यदि उन्होंने कबीर को पढ़ा तो क्या इन बातों पर उनकी नजर गई ? क्या उन्हें यह पता है कि राग, घरु, महला, भगत और गुरु, अंग और उलटबाँसी में रचनाएँ क्यों बँधी। कबीर की कविताओं के बंध-प्रबन्ध और ‘ग्रन्थ’ को पढ़ने वाले शिष्य नहीं, सिक्ख होते हैं ?
शिष्य और सिक्ख में क्या अन्तर है इसी तरह वाली छह सौ छियासी जातियाँ, अलख मुकामा और अलह मुकामा के अन्तर को कैसे तय करती हैं ? प्रकारान्ता से यह किताब अनजाने उन सारे हाथों तक भी पहुंचना चाहेगी जो कबीर को पढ़ने वालो को आलोचक कहते हैं। आलोचक का मतलब उनके लिए सही-सही देखना नहीं, निंदक होता है। पद्मपुराण से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक और शायद आज तक तय हो चुका है
कि संत या साधु की भूमिका में रहने वाला व्यक्ति चाहे घर-बारी हो, वैरागी हो, हिन्दु हो मुलसमान हो, सूफी हो, मलंग हो, जाति के कारण उपेक्षा का पात्र नहीं बनता। कबीर के समकालीन रैदास ने साफ-साफ लिखा-‘चारों वेद को कियो खण्डौति, ताको विप्र करें दण्डौति।’ क्या आकस्मिक है कि कबीर और रैदास एक बहुत बड़े समाज की पुस्तकों में संत और साधु की तरह स्थापित हैं। सभी संतों और साधुओं ने इस संसार को नश्वर, क्षणिक, मायामय कहा तो क्या उस संसार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, उन्हें सहेज, बचाकर नहीं रखा ?
क्या संतों ने कपड़ा बुनना छो़ड़ दिया, कटा हुआ माँस बेचना, हल जोतना, सिलाई करना, हजामत बनाना, एक खास कार्यक्रम के भीतर छोड़ दिया ? ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने पुराण, कुरान, पाखण्ड, पूजा, नमाज का विरोध किया तो उस समाज ने उन्हें छोड़ दिया। शब्द-सृजन के संसार में रहने वाले साधु अपनी बातों और हाथों के कारण, अपनी भीख नहीं, सीख के कारण प्रणाम प्राप्त करते हैं। न भी प्राप्त करें तो उनके शब्द, शब्दों के भीतर निहित कविता, अर्थ और तर्क सबका सिर झुका देते हैं। मेरा ख्याल है कि कबीर और उनकी तरह तमाम संतों की शब्द-योग्यता और प्रभाव-क्षमता पर ही बात होनी चाहिए। बेहतर तो होगा कि बात करने वाले करघे पर बैठें हों, राँपी से चमड़ा सिल रहे हों, उनके कंधे पर हल हो और बातों में दम हो,। ‘आसन मारि डिम्भ पर बैठे’ जैसे लोगों के लिए तो कबीर के यहाँ ही खारिज करने वाला ‘सबद-विवेक’ है।
इसलिए बहुत शाही अंदाज में ‘जोलहा से मटकऊवल’ अर्थात् कबीर से आँख मिचौनी नहीं हो सकती। चाहे, किसी के पास कितना भी सूत हो, कपास हो, चरखा हो, करघा हो। यह बात है कि ऐसे आदमी की पालकी मेरे कंधे पर है और ऐसे आदमी का तर्क मेरे लिए कोई रिडिल्स-पहेली नहीं होता। फिर भी यह सच है कि जब यशपाल जैसा लेखक ‘भगवान के पिता के दर्शन’ नामक कहानी लिखना है
या प्रेमचन्द को सरल भाषा का पाठ्यक्रम के योग्य लेखक मानता है। साफ-साफ कहता है कि प्रेमचन्द वर्ग-संघर्ष के विचारक नहीं, बल्कि जातीय संकीर्णताओं के विरोधी थे। प्रेमचन्द के मामले में ही नन्दुलारे बाजपेयी, श्रीनाथ सिंह, ज्योतिप्रसाद निर्मल और पंडित विद्यानिवास मिश्र का विरोध नहीं हुआ लेकिन हिन्दू-धर्म की पहेलियों पर सच लिखने के कारण बाबा साहब अम्बेडकर जैसे परम प्रतापी और सोहन पाल सुमनाक्षर जैसे साधारण साहित्यप्रेमी का भयंकर विरोध हुआ। देखना होगा कि विरोध करने वालों में कौन लोग थे ? क्या सभी सवर्ण थे ? प्रगतिशील नहीं थे ? प्रखर चिंतक तुलसीदास भी नहीं थे ? सभी थे। क्योंकि उन्हें प्रेमचन्द की स्थापित मर्यादा, एक बड़ा जन-समर्थन दे सकती थी। कबीर को लेकर जो नाकेबन्दी की जा रही है वह उत्साहवर्धक है, लेकिन इस नाकेबंदी के लिए मठों, विभिन्न सम्प्रदाय पोथियों की ओर से भी नजरे इनायात या नजरे-विलायत होनी चाहिए।
कबीर के पढ़ने का तरीका भी केवल किताबों से नहीं निकल सकता। उसके लिए नीव खोदने की पराकाष्ठा तक प्रयत्न किये बिना कबीर तक कैसे पहुँचा जा सकता है ? बंगाल के ‘बाऊल’ और कबीर के शब्द रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे गुरूदेव और पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे शान्तिनिकेतन आचार्य खड़ा करते हैं। इसी तरह यह देखना होगा कि उनके नाम से मिलने वाली असंख्य रचनाओं, कई भाव भंगिमाओं के बावजूद किस जतन से कबीर के असल को खोजा जाये। खोज जरूरी है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि खोज से सबकुछ मिल ही जाये।। मठों, पंथों के साथ-साथ निहंग लोगों में भी कबीर मिलते हैं। उसे भी जानना जरूरी है। भाषा में एक तदभवी जाति होती है। शुद्घ से अशुद्ध की ओर अर्थात् मिटते हुए की तुलना में बनते हुए की उर्जा।1 कबीर इसी बनने को बिगड़ना कहते हैं उन्हें पानी रहना है, गंगा नहीं, उन्हें लोहा रहना है, सोना नहीं, साधारण पेड़ रहना है, चंदन नहीं।
इस नहीं को समझे बिना कबीर के निकट कोई ‘हाँ’ या ‘एस’ नहीं हो सकता।
कबीर को लेकर एक वैचारिक दुनियाँ का निर्माण हुआ है जिसे विश्वविद्यालयों के अध्ययन में पाखण्ड की सीमा तक छोटे मुंह बड़ी बात के रूप में स्थापित किया गया। एक दूसरी दुनियाँ गायकों की है, जो सड़क से लेकर ओमकारनाथ ठाकुर ऐर कुमार गंधर्व क् ‘हममा, तुमम, सब मा बहुरि अकेला’ के अकेलेपन में है अथवा ‘जतन बताए जैहो, कइसे दिन कटिहैं।’ गंगा हो, चाहे जमुना इनके बीच में एक झोपड़ी बनाने के धुर पंचम में भी कबीर को सुनना होगा। एक हद वहाँ भी है जहाँ कबीर केवल सुनने की बात कहते हैं, कहना हो ही नहीं सकता। समझने की एक अन्तर्मुखी तड़प अर्थात् निरन्तर बैखरी से लौटते हुए परा तक पहुंचने वाली बेहद्दी की भूमिका होगी। इसे गूंगे का गुड़ या ‘समुझि मनहि मन रहिए’ की दशा भी कहा जा सकता है। इस दशा में पहुँचकर कहना सुनना खत्म हो जाता है।
कबीर के जन्म-मरण की तिथि का पचड़ा अभी तक तय नहीं हो पाया। कई तरह की बातें, कई उतार-चढ़ाव। चल यही रहा है कि 1398 में पैदा हुए और 120 वर्ष तक अर्थात् एक पूरी शताब्दी तक छाये रहे। संदेह मुक्त हुए या कुछ और हुआ। जिन्दगी भर ‘ना हिन्दू ना मुसलमान’ का अलख जगाया और अन्त में उनके बहुत प्यारे शिष्यों के पंथ और वंश के हिसाब से समाधि और रौजा खड़ा कर दिया।
मरने के साथ यह तय पाया कि ‘तू हिन्दू, तू मुसलमान।’ सौ साल से दो चार दिन पहले चुनार गढ़ के प० भानुप्रताप तिवारी ने जुगलानन्द कबीरपंथी को बताया कि वे विधवा-ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसे बिना किसी पुरुष-संसर्ग स्वामी रामानन्द के आशीर्वाद से पुत्रवती होने का वर मिला। लोक-लज्जा के भय से उसने लहरतारा के कमल-पत्र पर बच्चे को लिटा दिया।
यही बच्चा नीरु को पुत्र के रूप में मिला। नीरू अंसार, नीमा तुर्क। प्रतिलोम संताने इसी तरह नियति से गुजरती हैं। चाहे नारद जैसा ऋषि हो, अगस्त जैसा मुनि, चाहे कर्ण सहित कई भाई पाण्डव, व्यास तक। ये निजन्धर बड़े को छोटा करते हैं, छोटे को बड़ा। भारतीय मन की इस रचना-शैली में ‘कबीर’ शब्द का अर्थ ही होता है-‘सबसे बड़ा।’
कहीं पाठ की समस्या है, कहीं अर्थ की। कहीं अर्थ के अर्थ की। इसी तरह कहीं वेदान्ती हैं, कहीं निहंग। छह सौ साल से कुछ ज्यादा वर्ष हुए कबीर सारी दुनियाँ में भाषा के आर-पार सारंगी के तार में, खँज़ड़ी की छेड़छाड़ में, पाँव के घुँघरू में, करताल, खड़ताल, रेबाब, किंगरी और कुकुही में वचन नहीं, वाद्य हैं।
ऐसे विलक्षण व्यक्ति को जो छह सौ वर्षों से निरन्तर बन रहा है और तब तक बनता रहेगा जब तक आदमी अपने को ढंकते हुए, उभारते हुए, डरते हुए, डराते हुए, निर्भय नहीं हो जायेगा। इस कबीर की तलाश में पचास सालों के लिखित कुछ नमूने इस किताब में बिना किसी क्रम के प्रस्तुत हो रहे हैं। इसे विषयबद्ध भी किया जा सकता था, क्रमबद्ध भी लेकिन कबीर का कोई क्रम बन ही नहीं सकता वे सिलसिले से समझे जाने योग्य रचनाकार नहीं हैं। इसालिए उनकी सही सार्थक पढ़ाई के लिए उनको पढ़ते हुए हर पन्ने का एहसास अलग होना चाहिए।
कहीं कविता की दुनिया के अन्तिम व्यक्ति, कहीं लोगों का मन ही नहीं; दाँत भी खट्टाकर देने वाला साहस। लेकिन कबीर के बिना काम नहीं चल सकता। उनकी रचना के भी कई हजार रूप हैं और विवेचना के भी कई-कई लेकिन दोनों स्तरों पर कबीर को रचना ही पड़ता है। क्योंकि हर व्यक्ति की रचनाशीलता में ही कबीर ही रचनाशीलता है। इस किताब के बहाने कबीर का पढ़ना पढ़ा जा सकता है।
क्या है कबीर का पढ़ना ? इसको देखना है तो दलित-संज्ञान के प्रतिष्ठित लेखक, विद्वान् आई.ए.एस. बार-बार अपने को दलित कहने वाले डॉ० धर्मवीर पढ़ना ही देख लिया जा सकता है। उन्होंने तीन किताबें ‘कबीर के आलोचक’ पुस्तक-माला के रूप में लिखी हैं। कबीर को पढ़ने वाला कोई नहीं छूटा लेकिन सभी उन्हें कबीर के आलोचक लगते हैं, अध्येता नहीं। उनकी सारी मेहनत इस बात के लिए है कि कबीर को किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा। किसी को उनसे यह भी पूछना चाहिए कि आपने कबीर को कितना पढ़ा ? कैसे पढ़ा ? साखी क्या है ? वह दोहा है या दोहा नहीं है? सबद क्या है? वह शब्द है या पद? या दोनों नहीं है? रमैनी क्या है? उसमें जो बातें लिखी गईं हैं उनमें किस तरह की कम्यता है। चांचर, बेइल, बिरहुली, विप्रमतीसी चौंतीसा कहरा, चैती घांटो, फाग, बसंत, जंजीरा क्या है? इंगला, पिंगला, सुखमन तार क्या है? जुलाहा, कसाई, साधु पांडे, काजी, मुल्ला भाई क्यों उनकी कविता में हैं? फिर राग सोरठा में क्यों वह कहते हैं
कि मैं तो बिगड़ गया तुम नहीं बिगड़ना, हरा भरा पेड़ था चन्दन के संग चंदन होकर बिगड़ गया। निर्मल जल था गंगा के संग गंगा होकर बिगड़ गया। लोहा था पारस के संग सोना होकर बिगड़ा। कबीर था ओछा कसब वाला जुलाहा, राम के संग राम होकर बिगड़ा। क्या है इसका मतलब ? यह तो नहीं कि कोई बनता नहीं, सभी बिगड़ते ही हैं। यह तो नहीं कि किसी तरह का कवि–समय या मिथक या विश्वास केवल सपना होते हैं सच नहीं। इस तरह कबीर कई बार पलट कर देखते हैं
और अंत में ‘आइला गवनवाँ की बारी’ के विदा का गीत गाते हैं विवाह के रूपक में मौत का मुखौटा लगाते हैं। ठीक से बैठने को ‘उनमनी’ और ‘उदासी’ कहते हैं। उनकी कविता दुनियाँ की ओर जाती है या स्वर्ग, हेवन या किसी स्तर पर दोजख की ओर जाती है। कबीर की कविता से जुड़े हुए बहुत छोटे-छोटे सवाल हैं ? इनको हल करने के लिए भी कबीर को कितने लोगों ने पढ़ा ? मैं तो चार दशक से ज्यादा कबीर को पढ़ाते हुए इन सवालों से ही जूझता रहा। डॉ० धर्मवीर से मैं यह जानना चाहूंगा कि यदि उन्होंने कबीर को पढ़ा तो क्या इन बातों पर उनकी नजर गई ? क्या उन्हें यह पता है कि राग, घरु, महला, भगत और गुरु, अंग और उलटबाँसी में रचनाएँ क्यों बँधी। कबीर की कविताओं के बंध-प्रबन्ध और ‘ग्रन्थ’ को पढ़ने वाले शिष्य नहीं, सिक्ख होते हैं ?
शिष्य और सिक्ख में क्या अन्तर है इसी तरह वाली छह सौ छियासी जातियाँ, अलख मुकामा और अलह मुकामा के अन्तर को कैसे तय करती हैं ? प्रकारान्ता से यह किताब अनजाने उन सारे हाथों तक भी पहुंचना चाहेगी जो कबीर को पढ़ने वालो को आलोचक कहते हैं। आलोचक का मतलब उनके लिए सही-सही देखना नहीं, निंदक होता है। पद्मपुराण से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक और शायद आज तक तय हो चुका है
कि संत या साधु की भूमिका में रहने वाला व्यक्ति चाहे घर-बारी हो, वैरागी हो, हिन्दु हो मुलसमान हो, सूफी हो, मलंग हो, जाति के कारण उपेक्षा का पात्र नहीं बनता। कबीर के समकालीन रैदास ने साफ-साफ लिखा-‘चारों वेद को कियो खण्डौति, ताको विप्र करें दण्डौति।’ क्या आकस्मिक है कि कबीर और रैदास एक बहुत बड़े समाज की पुस्तकों में संत और साधु की तरह स्थापित हैं। सभी संतों और साधुओं ने इस संसार को नश्वर, क्षणिक, मायामय कहा तो क्या उस संसार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, उन्हें सहेज, बचाकर नहीं रखा ?
क्या संतों ने कपड़ा बुनना छो़ड़ दिया, कटा हुआ माँस बेचना, हल जोतना, सिलाई करना, हजामत बनाना, एक खास कार्यक्रम के भीतर छोड़ दिया ? ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने पुराण, कुरान, पाखण्ड, पूजा, नमाज का विरोध किया तो उस समाज ने उन्हें छोड़ दिया। शब्द-सृजन के संसार में रहने वाले साधु अपनी बातों और हाथों के कारण, अपनी भीख नहीं, सीख के कारण प्रणाम प्राप्त करते हैं। न भी प्राप्त करें तो उनके शब्द, शब्दों के भीतर निहित कविता, अर्थ और तर्क सबका सिर झुका देते हैं। मेरा ख्याल है कि कबीर और उनकी तरह तमाम संतों की शब्द-योग्यता और प्रभाव-क्षमता पर ही बात होनी चाहिए। बेहतर तो होगा कि बात करने वाले करघे पर बैठें हों, राँपी से चमड़ा सिल रहे हों, उनके कंधे पर हल हो और बातों में दम हो,। ‘आसन मारि डिम्भ पर बैठे’ जैसे लोगों के लिए तो कबीर के यहाँ ही खारिज करने वाला ‘सबद-विवेक’ है।
इसलिए बहुत शाही अंदाज में ‘जोलहा से मटकऊवल’ अर्थात् कबीर से आँख मिचौनी नहीं हो सकती। चाहे, किसी के पास कितना भी सूत हो, कपास हो, चरखा हो, करघा हो। यह बात है कि ऐसे आदमी की पालकी मेरे कंधे पर है और ऐसे आदमी का तर्क मेरे लिए कोई रिडिल्स-पहेली नहीं होता। फिर भी यह सच है कि जब यशपाल जैसा लेखक ‘भगवान के पिता के दर्शन’ नामक कहानी लिखना है
या प्रेमचन्द को सरल भाषा का पाठ्यक्रम के योग्य लेखक मानता है। साफ-साफ कहता है कि प्रेमचन्द वर्ग-संघर्ष के विचारक नहीं, बल्कि जातीय संकीर्णताओं के विरोधी थे। प्रेमचन्द के मामले में ही नन्दुलारे बाजपेयी, श्रीनाथ सिंह, ज्योतिप्रसाद निर्मल और पंडित विद्यानिवास मिश्र का विरोध नहीं हुआ लेकिन हिन्दू-धर्म की पहेलियों पर सच लिखने के कारण बाबा साहब अम्बेडकर जैसे परम प्रतापी और सोहन पाल सुमनाक्षर जैसे साधारण साहित्यप्रेमी का भयंकर विरोध हुआ। देखना होगा कि विरोध करने वालों में कौन लोग थे ? क्या सभी सवर्ण थे ? प्रगतिशील नहीं थे ? प्रखर चिंतक तुलसीदास भी नहीं थे ? सभी थे। क्योंकि उन्हें प्रेमचन्द की स्थापित मर्यादा, एक बड़ा जन-समर्थन दे सकती थी। कबीर को लेकर जो नाकेबन्दी की जा रही है वह उत्साहवर्धक है, लेकिन इस नाकेबंदी के लिए मठों, विभिन्न सम्प्रदाय पोथियों की ओर से भी नजरे इनायात या नजरे-विलायत होनी चाहिए।
कबीर के पढ़ने का तरीका भी केवल किताबों से नहीं निकल सकता। उसके लिए नीव खोदने की पराकाष्ठा तक प्रयत्न किये बिना कबीर तक कैसे पहुँचा जा सकता है ? बंगाल के ‘बाऊल’ और कबीर के शब्द रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे गुरूदेव और पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे शान्तिनिकेतन आचार्य खड़ा करते हैं। इसी तरह यह देखना होगा कि उनके नाम से मिलने वाली असंख्य रचनाओं, कई भाव भंगिमाओं के बावजूद किस जतन से कबीर के असल को खोजा जाये। खोज जरूरी है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि खोज से सबकुछ मिल ही जाये।। मठों, पंथों के साथ-साथ निहंग लोगों में भी कबीर मिलते हैं। उसे भी जानना जरूरी है। भाषा में एक तदभवी जाति होती है। शुद्घ से अशुद्ध की ओर अर्थात् मिटते हुए की तुलना में बनते हुए की उर्जा।1 कबीर इसी बनने को बिगड़ना कहते हैं उन्हें पानी रहना है, गंगा नहीं, उन्हें लोहा रहना है, सोना नहीं, साधारण पेड़ रहना है, चंदन नहीं।
इस नहीं को समझे बिना कबीर के निकट कोई ‘हाँ’ या ‘एस’ नहीं हो सकता।
कबीर को लेकर एक वैचारिक दुनियाँ का निर्माण हुआ है जिसे विश्वविद्यालयों के अध्ययन में पाखण्ड की सीमा तक छोटे मुंह बड़ी बात के रूप में स्थापित किया गया। एक दूसरी दुनियाँ गायकों की है, जो सड़क से लेकर ओमकारनाथ ठाकुर ऐर कुमार गंधर्व क् ‘हममा, तुमम, सब मा बहुरि अकेला’ के अकेलेपन में है अथवा ‘जतन बताए जैहो, कइसे दिन कटिहैं।’ गंगा हो, चाहे जमुना इनके बीच में एक झोपड़ी बनाने के धुर पंचम में भी कबीर को सुनना होगा। एक हद वहाँ भी है जहाँ कबीर केवल सुनने की बात कहते हैं, कहना हो ही नहीं सकता। समझने की एक अन्तर्मुखी तड़प अर्थात् निरन्तर बैखरी से लौटते हुए परा तक पहुंचने वाली बेहद्दी की भूमिका होगी। इसे गूंगे का गुड़ या ‘समुझि मनहि मन रहिए’ की दशा भी कहा जा सकता है। इस दशा में पहुँचकर कहना सुनना खत्म हो जाता है।
कबीर के जन्म-मरण की तिथि का पचड़ा अभी तक तय नहीं हो पाया। कई तरह की बातें, कई उतार-चढ़ाव। चल यही रहा है कि 1398 में पैदा हुए और 120 वर्ष तक अर्थात् एक पूरी शताब्दी तक छाये रहे। संदेह मुक्त हुए या कुछ और हुआ। जिन्दगी भर ‘ना हिन्दू ना मुसलमान’ का अलख जगाया और अन्त में उनके बहुत प्यारे शिष्यों के पंथ और वंश के हिसाब से समाधि और रौजा खड़ा कर दिया।
मरने के साथ यह तय पाया कि ‘तू हिन्दू, तू मुसलमान।’ सौ साल से दो चार दिन पहले चुनार गढ़ के प० भानुप्रताप तिवारी ने जुगलानन्द कबीरपंथी को बताया कि वे विधवा-ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसे बिना किसी पुरुष-संसर्ग स्वामी रामानन्द के आशीर्वाद से पुत्रवती होने का वर मिला। लोक-लज्जा के भय से उसने लहरतारा के कमल-पत्र पर बच्चे को लिटा दिया।
यही बच्चा नीरु को पुत्र के रूप में मिला। नीरू अंसार, नीमा तुर्क। प्रतिलोम संताने इसी तरह नियति से गुजरती हैं। चाहे नारद जैसा ऋषि हो, अगस्त जैसा मुनि, चाहे कर्ण सहित कई भाई पाण्डव, व्यास तक। ये निजन्धर बड़े को छोटा करते हैं, छोटे को बड़ा। भारतीय मन की इस रचना-शैली में ‘कबीर’ शब्द का अर्थ ही होता है-‘सबसे बड़ा।’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book